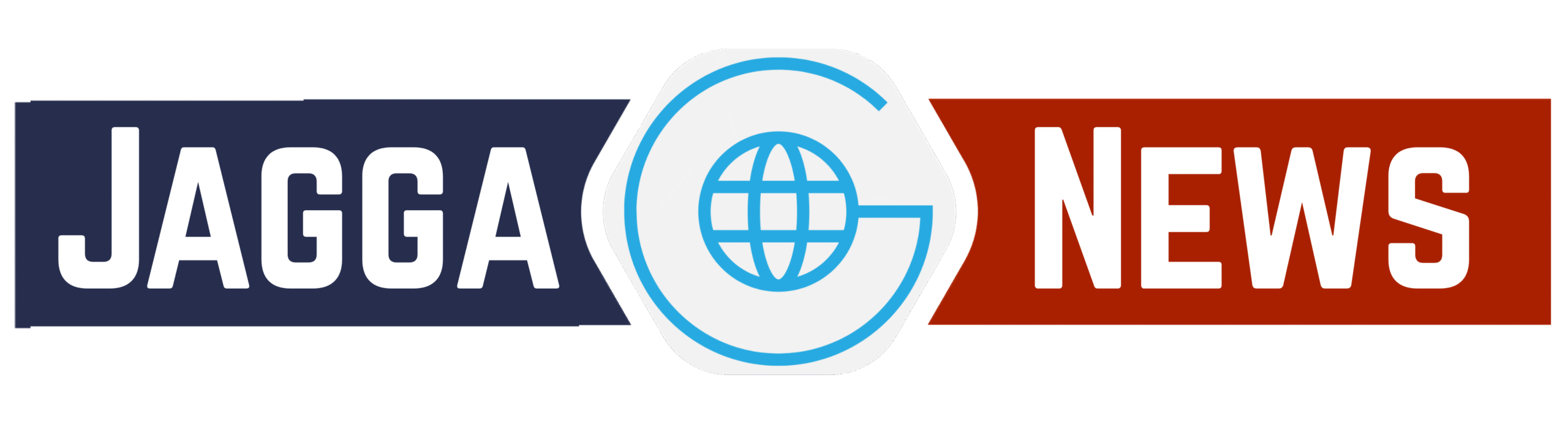उद्योगों में स्थानीय भागीदारी की चुनौतियां (30 अगस्त राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस पर विशेष)

छत्तीसगढ़ में एक नया बदलाव आते नजर आ रहा है इसी के साथ स्थानीय लोग हर ओर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते दिख पड़ रहें हैं। 30 अगस्त को ‘लघु उद्योग दिवस’ सन् 2000 से ही मनाया जा रहा है। भारत का छत्तीसगढ़ जहाँ खेती अब भी जीवन का मूल आधार है, लघु उद्योग प्राणवायु की तरह हैं। खासतौर पर कृषि और उससे जुड़े उत्पादों के प्रसंस्करण, भंडारण, पैकेजिंग, परिवहन, विपणन और निर्यात से संबंधित उद्योगों की संभावना सबसे अधिक है। यहां स्थानीय लोगों को इसकी भागीदारी सरकार सुनिश्चित कर सकती है। चीन तथा अमेरिका के आर्थिक मॉडल की नकल में एक ओर तो हम ‘सेज’ यानी स्पेशल इकोनामिक जोन और ‘एज’ यानी एग्रो एक्सपोर्ट जोन आदि भारी-भरकम औद्योगिक क्लस्टर स्थापित करने की मृग मरीचिका में भटकते रहे। जिस से स्थानीय लोगों की भागीदारी ख़त्म होती चली गई। अब हालात यहां तक आ पहुंचे हैं कि लघु-उद्योग लगाने की बात तो छोड़िए ‘लघु उद्योग-दिवस’ मनाने की औपचारिकता भी लगभग भूल गए हैं। फिर भी कोई नवउद्यमी गलती से अगर अपने गांव कस्बे में कोई लघु उद्योग लगाना चाहता है तब शुरू होती है असली राम-कहानी। 2024 के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक,इस घनघोर उपेक्षा के बावजूद देश के माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज क्षेत्र का भारत की जीडीपी में योगदान लगभग 30 फीसदी है, जबकि कुल निर्यात में यह हिस्सेदारी 43 फीसदी तक पहुँचती है। रोजगार सृजन में भी यह क्षेत्र अहम है। देश के कुल रोजगार का लगभग 110 मिलियन यहीं से आता है। चीन, वियतनाम जैसे देशों में यह योगदान भारत से कहीं अधिक है, जो बताता है कि हमारे सामने अवसर भी हैं और चुनौतियाँ भी। छत्तीसगढ़ ने अपनी औद्योगिक नीति 2024–29 में स्पष्ट किया है कि वह फूड प्रोसेसिंग, वुड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और नवीकरणीय ऊर्जा* जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। नीति में भूमि आवंटन, बिजली दरों में रियायत, ब्याज अनुदान, स्टार्टअप पैकेज जैसी कई सुविधाओं की बात कही गई है। दशकों पहले उद्योग लगाने के लिए कभी सिंगल विंडो’ की भी बात हुई थी,, जो अब शायद सेवन-विंडो’ में बदल गई है। कागज़ पर लिखी नीतियों और ज़मीनी हकीकत के बीच गहरी खाई है। केंद्र सरकार की नीति है कि ‘थर्मल पावर यूनिटें’ कम से कम पाँच प्रतिशत बायोमास जैसे लकड़ी या ब्रिकेट्स का उपयोग करें। प्रसंस्करण करने यह लकड़ी फर्नीचर के काम भी आ सकती है। इसके लिए भारत हर साल 35–40 हज़ार करोड़ रुपये की लकड़ी और टिंबर आयात करता है। यानी ऐसे उद्योग न सिर्फ़ आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ बन सकते हैं, बल्कि बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भी बचा सकते हैं। शायद इसीलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने नई औद्योगिक नीति में लकड़ी आधारित उद्योगों को बस्तर में प्राथमिकता श्रेणी में रखा। पर असली मज़ा तो यहीं से शुरू होता है। बस्तर के कुछ नवउद्यमी किसानों ने तय किया कि अपने आकेशिया प्लांटेशन फसल के प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन के लिए जगदलपुर के पास अपने खेतों पर एक छोटी सी इकाई डालेंगे। इससे इन्हें तथा इनके साथ जुड़े आकेशिया रोपण करने वाले अन्य किसानों को भी लाभ होगा, गांव के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। काम की शुरुआत हुई, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाई। क्योंकि सरकार अनुदान देने का दावा भी करती है। रिपोर्ट बनकर बैंक पहुँची, तो वहाँ से फरमान आया। ज़मीन कृषि भूमि है, पहले डायवर्ज़न कराइए।डायवर्ज़न के लिए राजस्व विभाग पहुँचे, तो उन्होंने कहा “ डायवर्सन तो हम करेंगे, पर पहले जरूरी विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेकर लाओ।” सबसे पहले ग्राम पंचायत की सहमति, दूसरा बिजली विभाग की सहमति, तीसरा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की सहमति, चौथाराष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की सहमति, पांचवां वन विभाग की सहमति, छठवां जिला उद्योग केंद्र में प्रोजेक्ट का पंजीयन,सातवा़ बैंक का एलओआई भी लगेगा जिससे आगे अनुदान मिलेगा। सबसे पहले तो शुरुआत में हर विभाग कहता है कि आप पहले बाकी विभागों से अनापत्ति लेकर आइए।जैसे कि, बिजली विभाग अगर कहे कि पहले आप ‘जिला उद्योग केंद्र’ में प्रोजेक्ट का पंजीयन करा कर लाइए और जब आप ‘जिला उद्योग केंद्र’ में रजिस्ट्रेशन के लिए जाएं तो वो कहें कि पहले आप हमें बिजली विभाग की अनापत्ति पत्र दिखाइए तो पंजीयन होगा। यानी पहले मुर्गी या पहले अंडा? ऐसे में बेचारा नवउद्यमी क्या करे? ग्राम पंचायत की अनापत्ति में चुनावी मनमुटाव के चलते पंचायत की राजनीति हावी हो गई। जहां कुटीर उद्योग और ग्रामीण विकास कहीं गुम हो गया। ग्राम पंचायत ने अपना अनापत्ति दे दी तो फिर बिजली विभाग आता है। बिजली विभाग तीन महीनों सर्वे करते रहते हैं। फिर महीने में ट्रांसफार्मर के लिए तथा लाइन के लिए टेंडर निकलेगा। बिजली और ट्रांसफार्मर लगवाने पर्याप्त सुविधा शुल्क देने के बावजूद कनेक्शन लेना कठिन है। वन-विभाग की भी एनओसी चाहिए। जो राष्ट्र हित और पर्यावरण संतुलन के लिए जरूरी है। फिर भी महीनों तक फ़ाइल अटकी रहती है। एक बात समझ से परे है कि किसान खुद की जमीन पर खुद मेहनत कर पेड़ लगाता है तो उसको काटने तथा परिवहन के लिए हमें एसडीएम , तहसीलदार, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, डिप्टी रेंजर, रेंजर डीएफओ तक चक्कर क्यों लगवाया जाता है। छत्तीसगढ़ का किसान पेड़ लगाने इस लिए ही कतराता है। उद्योग लगाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की एनओसी के बहुत सारे नियम हैं परियोजना स्थल हाईवे से 15 किमी दूर, आसपास गाँव है तो फिर उस गांव की भी अनुमति तो लेनी पड़ेगी। सबसे बड़ी कठिन समस्या आती है ‘टाउन एंड कंट्री प्लानिंग’ की एनओसी हासिल करने की। जहां इकाई लग रही है वहां न कोई टाउन है ना आने वाले बीसों साल तक किसी टाउन की प्लानिंग नहीं होनी चाहिए। स्पष्ट है कि लोकेशन शहर से 15 किलोमीटर दूर है, गांव तथा मोहल्ले भी दूर-दूर तक नहीं है। आसपास कोई रिहाइश या घर भी नहीं हो। जहां छोटी-मोटी सुविधा शुल्क से काम नहीं चलता नहीं तो नियम कायदे अड़ंगा बन जाते हैं। अंतिम स्वनाम-धन्य राजस्व- विभाग का सबसे पावरफुल अधिकारी जिला कलेक्टर होते हैं। कलेक्टर साहब से समय लेकर मिल सकते हैं पर पटवारी और तहसीलदार साहब से मिलना कठिन होता है। सुविधा शुल्क के बावजूद महीनों लटकाते है और का करके अहसान करते हैं। किसी भी छोटे-मोटे उद्योग को लगाने में आठ–दस महीने का चक्कर लगाना पड़ता है । कितने ही नवउद्यमी निराश होकर उद्योग लगाने का विचार ही छोड़ देते होंगे। अगर छोटे शहर गांव का कोई नवउद्यमी अपने गांव में सचमुच में कोई ‘लघु-उद्योग’ लगाना चाहता है तो ज़मीन का इंतज़ाम, पूंजी का इंतज़ाम, सात विभागों के तिलिस्म को तोड़कर सफलता पूर्वक उद्योग लगा लेता है तो वह अभिमन्यु के चक्रव्यूह भेदने से कम नहीं होता है। सरकार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर मीट आयोजित करती है। देश-विदेश के उद्योगपतियों के लिए लाल कालीन बिछाया जाता है।मुख्यमंत्री और मंत्रीगण बड़े-बड़े उद्योगपतियों से मिलते हैं, उन्हें तमाम तरह की सुविधा देने का वादा करके, समझौते साइन करते हैं। पर शायद ही कभी यह सोचते होंगे कि गांव तहसील स्तर पर एक छोटा सा उद्योग लगाने को इच्छुक एक छोटे उद्यमी को किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। छत्तीसगढ़ सरकार हर ओर आमूल चूल परिवर्तन कर रही है। छत्तीसगढ़ के लोगों को बढ़ावा देने के लिए जरूरी क़दम भी उठा रही है जिसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में स्थानीय लोगों के छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार सिंगल विंडो प्रणाली को मूर्तरूप प्रदान करे तो यह बेहतरीन पहल होगी। जिसके चलते स्थानीय लोगों को की आय बढेगी और समग्र ग्रामीण विकास भी मार्ग प्रशस्त होगा।

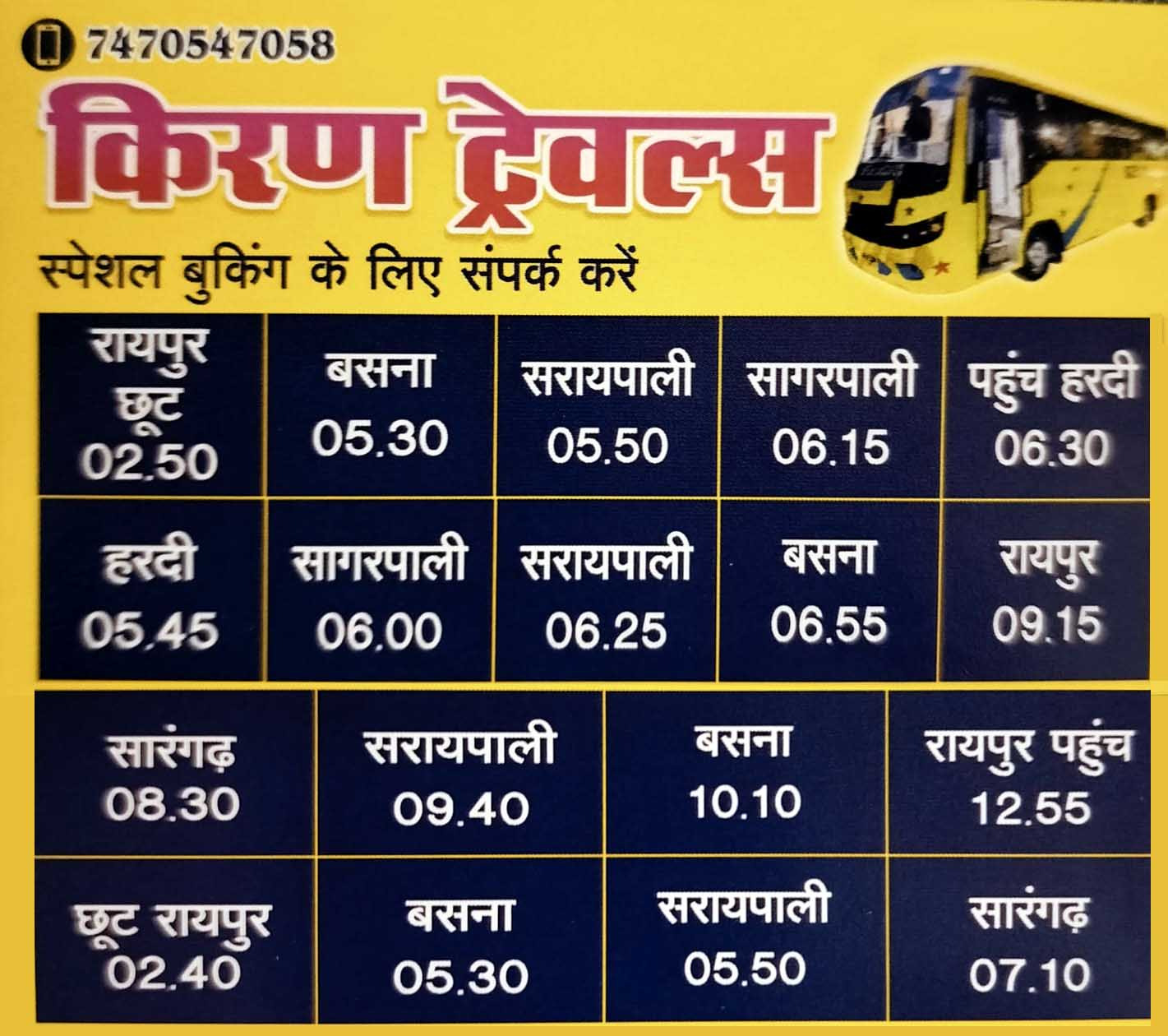
लेखक: डॉ. राजाराम त्रिपाठी,अखिल भारतीय किसान महासंघ ‘आईफा’ के राष्ट्रीय संयोजक